Types of Banks in India: प्रभावशाली सकारात्मक रूप
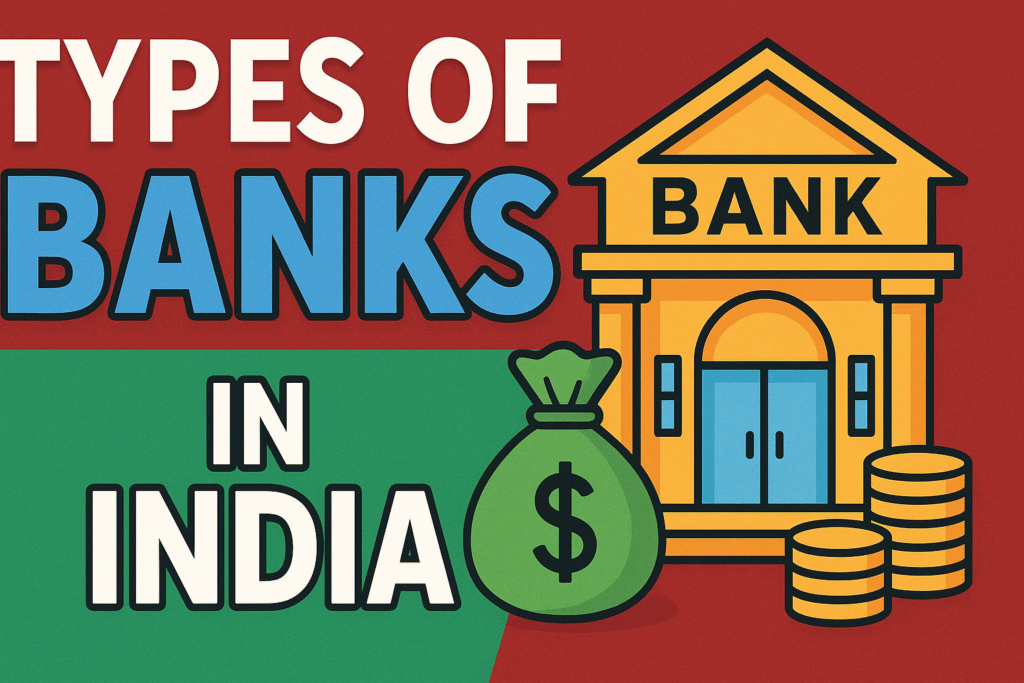
परिचय: आपके UPSC सपने के लिए बैंक क्यों मायने रखते हैं
भारतीय बैंकिंग प्रणाली सिर्फ़ आपके पैसे रखने की जगह नहीं है; यह हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़, और आपके यूपीएससी, राज्य पीएससी और अन्य सरकारी नौकरी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्व का विषय है। प्रारंभिक जहाँ बैंक के प्रकार, कार्यों और विनियमों पर सीधे प्रश्न आम हैं,मेन्स जहां आप आर्थिक विकास, वित्तीय समावेशन और सामाजिक योजनाओं में उनकी भूमिका का विश्लेषण करेंगे, इस विषय की गहरी समझ अनिवार्य है।
यह गाइड न केवल आपको तथ्यों को याद रखने में मदद करेगी, बल्कि आपके उत्तरों को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक विश्लेषणात्मक गहराई भी प्रदान करेगी। आइए, भारतीय बैंकिंग परिदृश्य को समझें और जटिल अवधारणाओं को सरल बनाएं ताकि आप उनमें महारत हासिल कर सकें।
ऐतिहासिक संदर्भ: भारत में बैंकिंग का विकास
भारत में बैंकिंग का इतिहास एक रोचक यात्रा है जो देश के आर्थिक और राजनीतिक विकास को प्रतिबिंबित करती है। इसे मोटे तौर पर तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है:
चरण I: स्वतंत्रता-पूर्व काल (1947 से पहले):इस युग में बैंक ऑफ हिन्दुस्तान (1770) जैसे औपनिवेशिक काल के बैंकों की स्थापना हुई। तीन प्रेसीडेंसी बैंकों—बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास—का बाद में 1921 में विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, जो अंततः भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई)इस अवधि को केंद्रीय बैंकिंग प्राधिकरण की कमी के लिए जाना जाता है।
चरण II: स्वतंत्रता के बाद की अवधि (1947-1991):सरकार का ध्यान विकास और वित्तीय समावेशन की ओर स्थानांतरित हो गया।
राष्ट्रीयकरण:1969 में 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों और 1980 में 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के ऐतिहासिक निर्णय का उद्देश्य कृषि और लघु उद्योगों जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराना था, जिससे लाभ से ध्यान हटाकर सामाजिक कल्याण पर केंद्रित किया जा सके।
आरबीआई का गठन:दभारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) इसकी स्थापना 1935 में हुई थी और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिससे इसे भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका मिली।
चरण III: उदारीकरण अवधि (1991 के बाद):1991 के आर्थिक सुधारों ने निजी और विदेशी बैंकों के लिए द्वार खोले, जिससे प्रतिस्पर्धा, दक्षता और नई तकनीकों का आगमन बढ़ा। इस अवधि को नियामक सुधारों और नए प्रकार के बैंकों के उद्भव के लिए भी प्रोत्साहित किया गया।
भारत में बैंकों का व्यापक वर्गीकरण
भारत में बैंकों को उनके कार्यों और संरचना के आधार पर व्यापक रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। इस वर्गीकरण की स्पष्ट समझ आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
A. केंद्रीय बैंक: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
‘बैंकों का बैंक’: भारतीय रिजर्व बैंक भारत की सर्वोच्च बैंकिंग संस्था है। यह कोई वाणिज्यिक बैंक नहीं है; यह जनता से जमा स्वीकार नहीं करता।
महत्वपूर्ण कार्यों:
मौद्रिक प्राधिकरण:मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए धन की आपूर्ति को नियंत्रित करता है, ब्याज दरों (रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, आदि) का प्रबंधन करता है।
नियामक एवं पर्यवेक्षक:जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली की देखरेख करना।
मुद्रा जारीकर्ता:भारत में मुद्रा जारी करने और उसका प्रबंधन करने का एकमात्र प्राधिकारी।
सरकार का बैंकर:सरकार के बैंकिंग लेनदेन का प्रबंधन करता है।

B. Commercial Banks: The Heartbeat of the Economy
These are profit-making institutions that accept deposits and provide loans. They form the core of India’s banking system.
| Type of Commercial Bank | Key Characteristics |
|---|---|
| Public Sector Banks | Majority stake (over 50%) is held by the government. Examples: SBI, Punjab National Bank (PNB). Focus on both profit and social objectives. |
| Private Sector Banks | Majority stake is held by private individuals/entities. Examples: HDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank. Focus on profitability and efficiency. |
| Foreign Banks | Banks with their headquarters outside India but operating branches in India. Examples: Citibank, Standard Chartered Bank. Often specialize in foreign exchange and international banking. |
| Regional Rural Banks (RRBs) | Established to serve rural areas with credit. Owned jointly by the Central Government, State Government, and Sponsor Bank. Example: Prathama Grameen Bank. |
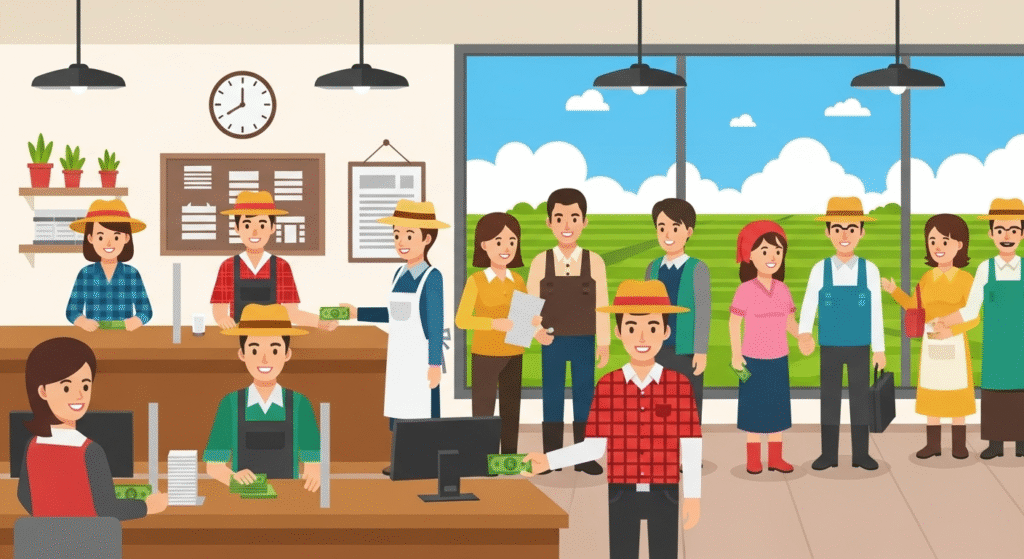
सी. सहकारी बैंक: जमीनी स्तर पर बैंकिंग
उद्देश्य:जनता द्वारा जनता के लिए गठित इन बैंकों का विनियमन भारतीय रिजर्व बैंक तथा संबंधित राज्य सहकारी समितियों के अधिनियमों द्वारा किया जाता है।
संरचना:वे तीन स्तरीय प्रणाली पर काम करते हैं:
राज्य सहकारी बैंक (राज्य स्तर पर)
केंद्रीय/जिला सहकारी बैंक (जिला स्तर पर)
प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (ग्राम स्तर पर)
सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव:वे ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में किसानों और छोटे व्यवसायों को ऋण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
डी. विशिष्ट बैंक: विशिष्ट अंतरालों को भरना
ये बैंक विशिष्ट क्षेत्रों या आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं।
विकास बैंक:बड़ी परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करें। उदाहरण:NABARD(राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक),सिडबी(भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक),एक्जिम बैंक(भारतीय निर्यात-आयात बैंक)।
भुगतान बैंक:बैंकों का एक नया वर्ग जो एक निश्चित सीमा (वर्तमान में ₹2 लाख) तक जमा स्वीकार कर सकता है, लेकिन ऋण या क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता। उदाहरण: एयरटेल पेमेंट्स बैंक। इनका ध्यान डिजिटल लेनदेन और वित्तीय समावेशन पर है।
लघु वित्त बैंक:छोटे व्यवसायों, छोटे और सीमांत किसानों, और सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों सहित समाज के वंचित और कम सेवा प्राप्त वर्गों को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना। उदाहरण: इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक।
आर्थिक और सामाजिक महत्व: पाठ्यपुस्तक से परे
‘क्या’ के पीछे ‘क्यों’ को समझना एक अच्छे मुख्य परीक्षा उत्तर की कुंजी है।
वित्तीय समावेशन:विभिन्न प्रकार के बैंकों, विशेषकर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और भुगतान बैंकों का प्रसार, इसके विकास का एक प्रमुख कारण रहा है।वित्तीय समावेशन. जैसे कार्यक्रम Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY)इस नेटवर्क का लाभ उठाकर लाखों बैंकिंग सेवाओं से वंचित नागरिकों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाया गया है।
आर्थिक प्रभाव:बैंकिंग क्षेत्र आर्थिक विकास का इंजन है। बचत को जुटाकर और उसे उत्पादक क्षेत्रों में ऋण के रूप में पहुँचाकर, बैंक निवेश, उपभोग और रोज़गार सृजन को बढ़ावा देते हैं।
उम्मीदवारों के लिए चिंताजनक बिंदु:कई छात्रों को विभिन्न प्रकार के बैंकों की सूक्ष्म बारीकियों में अंतर करना मुश्किल लगता है। जल्दी से दोहराने और तुलना करने के लिए अपने नोट्स में एक तालिका (ऊपर दी गई तालिका की तरह!) बनाना न भूलें।
केस स्टडी: एनपीए संकट और बैंकिंग सुधार
इसकी समस्या गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनपीए)भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के सामने एक बड़ी चुनौती है। एनपीए एक ऐसा ऋण या अग्रिम होता है जिसका मूलधन या ब्याज भुगतान 90 दिनों की अवधि तक बकाया रहता है।
आर्थिक निहितार्थ:उच्च एनपीए से बैंक की लाभप्रदता और ऋण देने की क्षमता प्रभावित होती है, जिससे आर्थिक विकास धीमा हो जाता है।
सरकार की प्रतिक्रिया:सरकार और आरबीआई ने कई उपाय शुरू किए हैं जैसे दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी)और इस समस्या के समाधान के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण। यह एक ऐसे विषय का उत्कृष्ट उदाहरण है जिसका विश्लेषण आप अपनी मुख्य परीक्षा के उत्तर के लिए कई दृष्टिकोणों से कर सकते हैं।
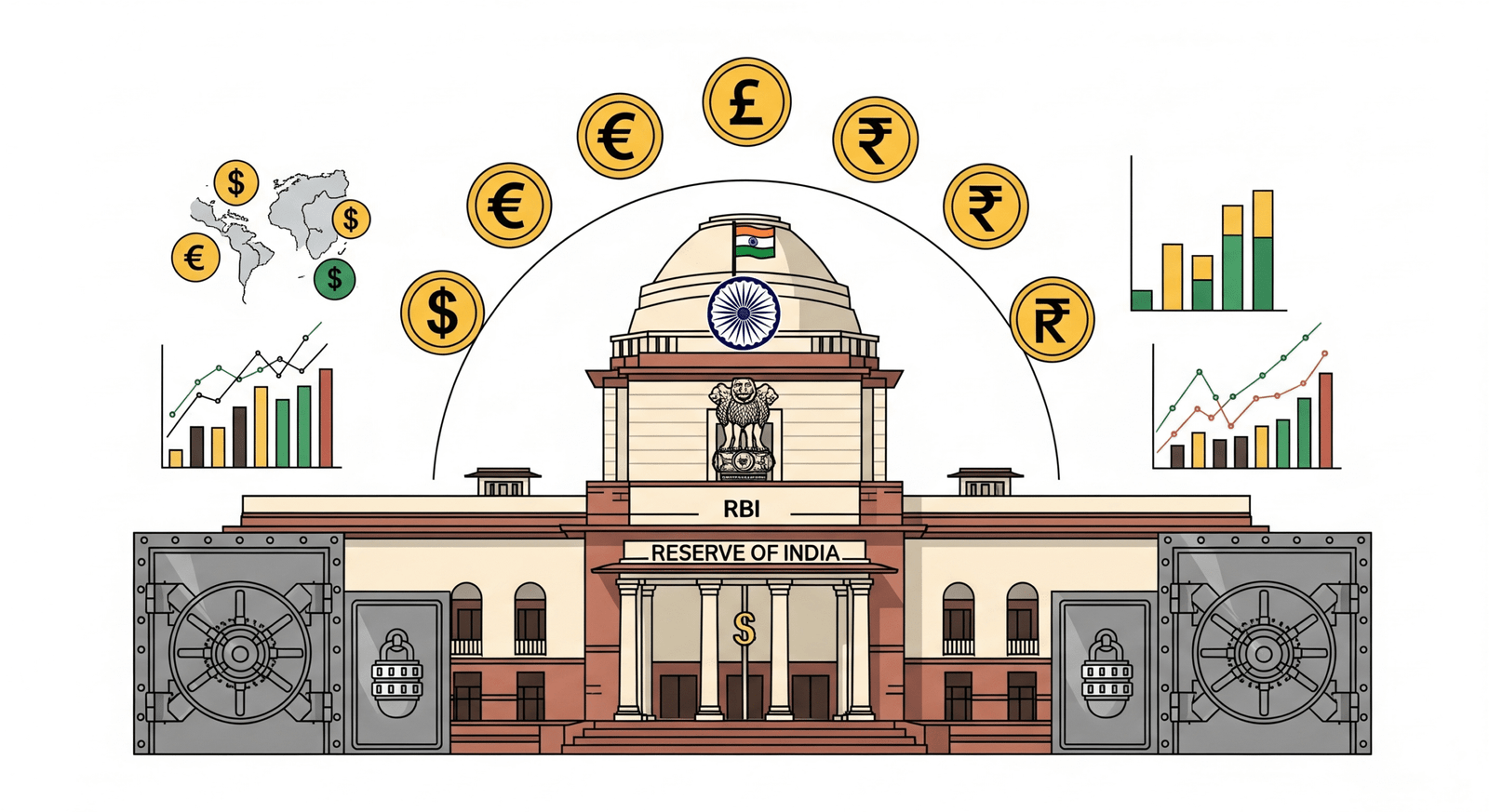
निष्कर्ष: आपकी सफलता का रोडमैप
भारतीय बैंकिंग प्रणाली में महारत हासिल करना सिर्फ़ अंक हासिल करने के बारे में नहीं है; यह आपके देश की वित्तीय संरचना को समझने के बारे में है। बैंकों के प्रकारों, उनके कार्यों और उनकी चुनौतियों के बारे में आपका ज्ञान एक सिविल सेवक के रूप में आपकी भूमिका में अमूल्य होगा, चाहे आप ग्रामीण विकास, वित्तीय नीति या लोक प्रशासन पर काम कर रहे हों।
उम्मीदवारों के लिए तैयारी के सुझाव:
प्रारंभिक परीक्षा:तथ्यात्मक विवरणों पर ध्यान केंद्रित करें – बैंकों के नाम, उनके संस्थापक, स्थापना के वर्ष (जैसे, आरबीआई) और प्रत्येक बैंक प्रकार के विशिष्ट कार्य।
मुख्य परीक्षा:समग्र दृष्टिकोण अपनाएं। विषय को आर्थिक सुधार, वित्तीय समावेशन और आरबीआई की भूमिका जैसे व्यापक विषयों से जुड़े। आंकड़ों और सरकारी रिपोर्टों (जैसे आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट) अपने बिंदुओं को प्रमाणित करने के लिए।
साक्षात्कार:हालिया बैंकिंग समाचार, नई प्रौद्योगिकियों (जैसे यूपीआई) के प्रभाव और इस क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए तैयार रहें।
याद रखें, आप जो भी अवधारणा सीखते हैं, वह आपके लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ाती है। हज़ार मील का सफ़र एक कदम से शुरू होता है। सीखते रहो, बढ़ते रहो!आप यह कर सकते हैं!
