पंचायती राज व्यवस्था: ग्रामीण भारत का अद्भुत विकास!
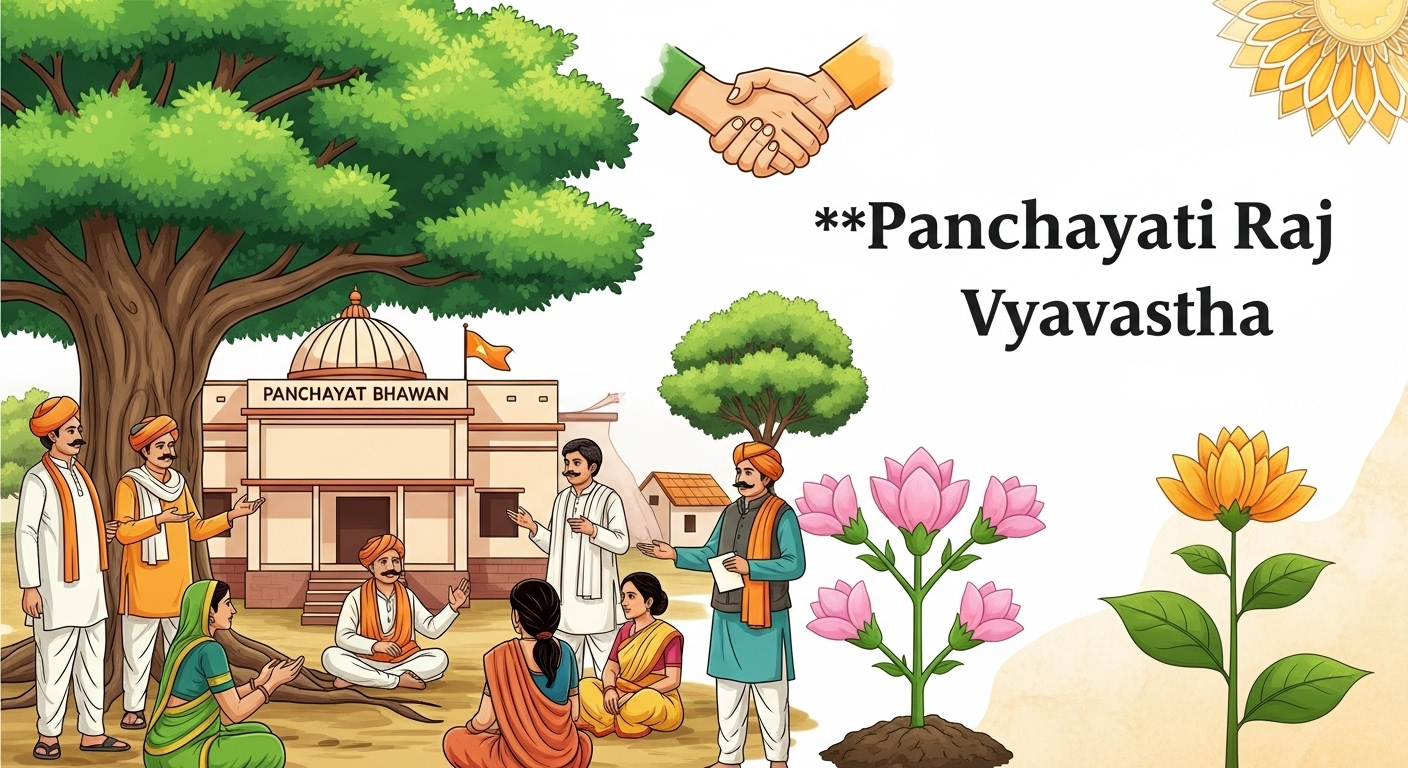
परिचय: प्राचीन जड़ों से आधुनिक शासन तक
क्या आपने कभी सोचा है कि किसी देश की नींव में लोकतंत्र कैसे काम करता है? भारत में, वह नींव है “पंचायती राज व्यवस्था यानि स्थानीय स्वशासन” यह शासन का विकेन्द्रीकृत स्वरूप है जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सीधे सत्ता प्रदान करता है, इसे ग्रामीण विकास का दायित्व सौंपा गया है जिससे महात्मा गांधी का सपना साकार होता है।”Gram Swaraj”—ग्राम स्वशासन—को हकीकत में बदलना। यूपीएससी, राज्य पीसीएस या अन्य सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे किसी भी उम्मीदवार के लिए, इस विषय की गहरी समझ होना अनिवार्य है, क्योंकि यह भारतीय राजनीति और शासन का एक महत्वपूर्ण तत्व है।
यह लेख ऐतिहासिक संदर्भ, संवैधानिक प्रावधानों और आधुनिक चुनौतियों को एकीकृत करके पंचायती राज व्यवस्था के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका प्रस्तुत करता है। आप इसकी प्राचीन उत्पत्ति, इसे आकार देने वाली ऐतिहासिक समितियों, महत्वपूर्ण 73वें संविधान संशोधन और उन चुनौतियों के बारे में जानेंगे जो इसकी पूर्ण क्षमता को साकार होने से रोकती हैं।
स्थानीय स्वशासन का ऐतिहासिक विकास
भारत में स्थानीय स्वशासन की अवधारणा कोई नई बात नहीं है; इसका इतिहास हजारों वर्षों से भी अधिक पुराना है।
प्राचीन भारत: साक्ष्य ऋग्वेद ग्राम परिषदों का उल्लेख है जिन्हें के रूप में जाना जाता है “Sabhas” और “Samitis”जो गाँव के मामलों का प्रबंधन करते थे। कौटिल्य जैसे ग्रंथArthashastra ग्राम प्रधानों की प्रशासनिक भूमिका का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। ये परिषदें स्थानीय स्तर पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने और विवादों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं।
मध्यकाल:केंद्रीय साम्राज्यों के उदय के बावजूद, गाँवों की स्वायत्तता काफी हद तक बनी रही। स्थानीय स्वशासन ने गाँव-स्तर के मुद्दों को संभालना जारी रखा, हालाँकि कभी-कभी सामंती भूमि व्यवस्थाओं के कारण इसकी शक्तियाँ सीमित हो जाती थीं।
British Era:अंग्रेजों ने स्थानीय शासन की एक अधिक औपचारिक, लेकिन शुरुआत में सीमित प्रणाली शुरू की। लॉर्ड रिपन की 1882 का संकल्प इसे “भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा” कहा जाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना था। हालाँकि, यह मुख्यतः प्रशासनिक सुविधा के लिए था, न कि विकेंद्रीकरण के किसी वास्तविक प्रयास के लिए।भारत सरकार अधिनियम, 1919, और यह भारत सरकार अधिनियम, 1935, ने स्थानीय शासन को और बढ़ावा दिया, लेकिन यह अभी भी एक अधीनस्थ कार्य था।
स्वतंत्रता के बाद की बहस:भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद, महात्मा गांधी, जिन्होंने गांवों को शासन की आदर्श इकाई के रूप में स्थापित करने की वकालत की, और डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, जिन्होंने ग्राम स्तर पर संभावित जाति-आधारित असमानताओं के बारे में चिंता व्यक्त की। इसके परिणामस्वरूप पंचायतों को भी इसमें शामिल किया गया।राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (अनुच्छेद 40)संविधान के न्यायोचित भाग के बजाय।

ऐतिहासिक समितियाँ और उनकी सिफारिशें
स्थानीय शासन का अध्ययन करने के लिए नियुक्त कई समितियों द्वारा संवैधानिक दर्जा का मार्ग प्रशस्त किया गया।
बलवंत राय मेहता समिति (1957):इस समिति की सिफ़ारिशें अभूतपूर्व थीं। इसने पंचायती राज के लिए त्रि-स्तरीय ढाँचे का प्रस्ताव रखा:
Gram Panchayat गांव स्तर पर.
Panchayat Samiti ब्लॉक/मध्यवर्ती स्तर पर।
Zila Parishad जिला स्तर पर। राजस्थान इस प्रणाली को अपनाने वाला पहला राज्य था, उसके बाद आंध्र प्रदेश का स्थान था।
अशोक मेहता समिति (1977):पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज की समीक्षा के लिए नियुक्त इस समिति ने दो स्तरीय प्रणाली की सिफारिश की तथा पंचायत चुनावों में राजनीतिक दलों की भागीदारी की वकालत की।
73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992: निर्णायक मोड़
73वां संशोधन एक ऐतिहासिक कदम था जिसने पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) PRI को संवैधानिक दर्जा दिया। इसमें कहा गया भाग IX(अनुच्छेद 243 से 243-ओ) और ग्यारहवीं अनुसूची संविधान में। यह अधिनियम 1948 से लागू हुआ।24 अप्रैल, 1993, जिसे अब मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस.
73वें संशोधन के प्रमुख प्रावधान
अनिवार्य प्रावधान:
त्रि-स्तरीय प्रणाली:20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी राज्यों के लिए अनिवार्य।
Gram Sabha:गाँव के सभी पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर बनी एक आधारभूत संस्था। यह ग्राम स्तर पर विधान सभा के रूप में कार्य करती है, जो विकास योजनाओं और बजट को मंजूरी देने के लिए ज़िम्मेदार है।
सीटों का आरक्षण:आरक्षण को अनिवार्य करने वाला एक महत्वपूर्ण प्रावधान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और औरत(कम से कम एक तिहाई सीटें) हाशिए पर पड़े समूहों को शामिल करना सुनिश्चित करना।
निश्चित अवधि:पंचायतों का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है। यदि पंचायतें भंग हो जाती हैं, तो छह महीने के भीतर नए चुनाव कराने होंगे।
राज्य चुनाव आयोग:पंचायत चुनावों के संचालन और देखरेख के लिए गठित एक स्वतंत्र निकाय।
राज्य वित्त आयोग:पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और निधि आवंटन की सिफारिश करने के लिए हर पांच साल में नियुक्त किया जाता है।
ग्यारहवीं अनुसूची:इस अनुसूची में सूचीबद्ध हैं 29 कार्यात्मक वस्तुएँ(कृषि, पेयजल, सड़क, ग्रामीण आवास और स्वास्थ्य जैसे विषय) जिन्हें पंचायतों को हस्तांतरित किया जाना है।
पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा)
जनजातीय समुदायों के अनूठे रीति-रिवाजों और परंपराओं को मान्यता देते हुए सरकार ने अधिनियम बनाया। पेसा अधिनियम, 1996 इसका प्राथमिक उद्देश्य जनजातीय स्वशासन की रक्षा करते हुए 73वें संशोधन के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करना था।
मूल सिद्धांत:यह जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाता है ग्राम सभा अंतिम प्राधिकारी लघु वनोपज, भूमि अधिग्रहण और स्थानीय संसाधनों के प्रबंधन जैसे मामलों पर। इस अधिनियम का उद्देश्य आदिवासियों की भूमि के हस्तांतरण को रोकना और उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना है।
पंचायती राज के लिए चुनौतियाँ और आगे का रास्ता
संवैधानिक समर्थन के बावजूद, पंचायतों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो उन्हें अपनी पूरी क्षमता हासिल करने से रोकती हैं।
| Challenges | Way Forward |
|---|---|
| Lack of Funds: Over-reliance on government grants. Most states have not devolved all 29 subjects and financial powers. | Empower PRIs to levy and collect local taxes. Increase untied grants from the Central and State governments. |
| Lack of Autonomy: Interference from local MLAs, MPs, and bureaucracy. State governments are often reluctant to devolve full powers. | Full devolution of the 3Fs: Funds, Functions, and Functionaries. Strengthen the role of Gram Sabhas. |
| Inadequate Staff & Infrastructure: Lack of trained personnel and basic infrastructure to carry out administrative tasks. | Capacity building and training programs for elected representatives. Appoint dedicated staff for Panchayats. |
| Social Hierarchies: The persistence of caste and gender biases, leading to "proxy" representation. | Strengthen social audit mechanisms. Increase awareness and education among villagers, especially women. |
| Lack of Transparency: Cases of corruption and misuse of funds are reported due to weak audit systems. | Implement e-governance initiatives like e-Gram Swaraj to ensure transparency and accountability in financial transactions. |
निष्कर्ष: लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करना
पंचायती राज व्यवस्था की यात्रा महत्वपूर्ण प्रगति और निरंतर चुनौतियों से भरी रही है। प्राचीन ग्राम परिषदों से लेकर संवैधानिक रूप से अनिवार्य तृतीय स्तर की सरकार तक, यह भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सबसे प्रभावी साधन बन गई है। हालाँकि वित्तीय निर्भरता और नौकरशाही नियंत्रण जैसे मुद्दे अभी भी मौजूद हैं, लेकिन नागरिकों को सशक्त बनाने और समावेशी विकास को गति देने की इस प्रणाली की क्षमता निर्विवाद है उम्मीदवारों के लिए, इस विषय के प्रति आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेखों और समितियों को रटने से आगे बढ़ें; समाज पर व्यवस्था के प्रभाव, उसकी चुनौतियों और उसके भविष्य को समझें। भारतीय लोकतंत्र का भविष्य उसके गाँवों में निहित है, और इस विषय की आपकी समझ एक मज़बूत और अधिक विकेंद्रीकृत भारत की दिशा में एक कदम है।